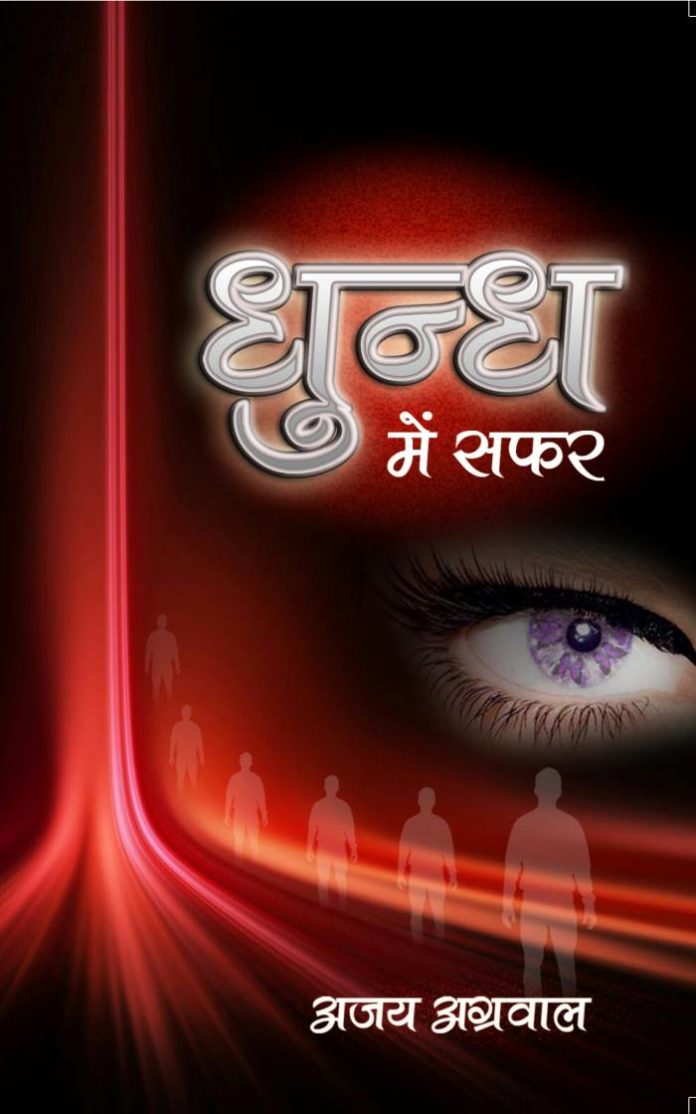अजय अग्रवाल का उपन्यास “धुन्ध में सफर “
- समीक्षा – काव्या पब्लिकेशंस , दिल्ली / भोपाल मूल्य केवल 160.00 यह किताब Amazon पर भी उपलब्ध है
अजय अग्रवाल की औपन्यासिक कृति “धुन्ध में सफर “ जिस वैचारिक प्रवाह को अपने में समेटे है , वह इस कृति के शीर्षक को अक्षरशः सार्थक सिद्ध करता है. धुन्ध वह एक स्थिति है जिसमें कुछ भी प्रथम दृष्टया उजागर नहीं हो पाता. विचारों पर धुन्ध का रहना मानव जाति के लिए विनाशक तो है ही, भविष्य के लिए भी दिशा का निर्धारण करने में बाधक है. यह एक ऐसी विषैली मनःस्थिति है जिसके रहते समाज में घातक उथलपुथल का सिलसिला अस्तित्व में रहता है . पात्रों और स्थितियों की मौजूदगी के चलते अजय ने इसे बखूबी प्रदर्शित किया है.
धुन्ध में कोई भी चेहरा, कोई भी अक्श उजागर नहीं होता. सारी स्थितियां अधुरी और अस्पष्ट बनी रहती हैं. यथार्थ में भले ही कोई ईमानदार भी है और समर्पित भी और कर्तव्यनिष्ठ भी , फिर भी आधा अधूरा इसलिए है क्योंकि जो उसके पास होना चाहिए, वह नहीं है.
राजनेता सत्ता का इस्तेमाल किसी सेवाभावना, अर्पण समर्पण के भाव से उद्दीप्त होकर नहीं अपितु एक ऐसे औजार के रूप में करता है जो धनागम का अनवरत जरिया बन सके. वह कानून खरीदने में सक्षम है. पुलिस है, जो उसके इशारों में घूमती है. विवश जनता सत्य से परिचित होती हुई भी उसके खिलाफ नहीं जा पाती.
लेखक की यह कृति युवा भारत के लिए , युवामानस के लिए समर्पित है. कोर्ट कचहरी की दलीलों और आत्मकथ्य से प्रारंभ हुआ कथानक इस एक वाक्य पर आ रूकता है: कोर्ट इज़ एडजर्न्ड टिल डेसीजन . अंतिम पंक्ति आजाद देश में सात दशकों में विकसित हुए सत्य को परिभाषित करती है. ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता के समक्ष सभी बौने बने हुए हैं. कोई स्पष्ट रूप से उससे नाराज़गी नहीं पालना चाहता. लेकिन एक निष्कर्ष यह भी तो उभरकर आता है कि: युद्धरत तो होना ही पड़ेगा, अपनों से अपनों के खिलाफ ! फिर चाहे कोई प्रभातकुमार हो, उमाशंकर हो, गजराज हो, नरसिंहदेव या सत्यप्रकाश हो या कुलदीप सिंह हो या फिर सुबोधकांत ! एक दूसरे से भिड़ना तभी अनिवार्य हो जाता है, जब मूल्य बलि पर चढ़ने के लिए बाध्य हों!
धुन्ध के इससफर में एक भीनी-भीनी मध्यम-मध्यम प्रेम के सूर की अनुगूंज भी है, जिसके मंतव्य को समझना पड़ता है. यह अनुगूंज ठीक वैसी ही प्रतीत होती है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी: उसने कहा था में सुनने को मिलती है या फिर शशिकपूर की कालजयी फिल्म जूनून में! प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता. प्रेम की संप्राप्ति का अप्रतिम स्वर है. त्याग! इस उपन्यास में जूनून की हद तक यही स्वर तो आगे बढ़ता है और कथ्य को दिशा प्रदान करने का माध्यम बनता है. इसके लिए कोई शक्ल अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. प्रेम तटस्थ होता है , यह मौसम के बदलने की रीत नहीं समझता. सारिका का प्रभात के प्रति प्रेम इसी पंक्ति का प्रेम है: तटस्थ और समर्पित ! यह अदृश्य प्रेम है. इस प्रेम का सफर बहुत ही पाक है. यहां तक कि सारिका अपने पति कार्तिक को अपने प्रिय प्रभात के मिशन में शामिल होने की प्रेरणा देती हैं. भले ही उसका प्रेम अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवारजनों से टकराता है लेकिन ऐसा होने पर भी कदापि धूमिल नहीं पड़ता. इसमें एक सी रवानगी व्याप्त रहती है. यह एक दूसरे के लिए संबल भी है और एक नवबीज की रचना का आधार भी.
‘ धुंध ’ के इस सफर में कई उतार चढ़ाव हैं. प्रभातकुमार के पास डाक्टर की निर्धारित डिग्री भले ही न हो, लेकिन मरीज के प्रति सेवा समर्पण का भाव अवश्य विद्यमान है. इसी स्वर की वज़ह से वह सामाजिकों में अपनी जगह बनाए हुए है. लेकिन जैसे कानून सबूत मांगता है , ठीक वैसे ही डाक्टर के लिए भी डाक्टरी की डिग्री चाहिए ही. सारे उपन्यास का तानाबाना इसी के अंतर्गत बुना गया है.
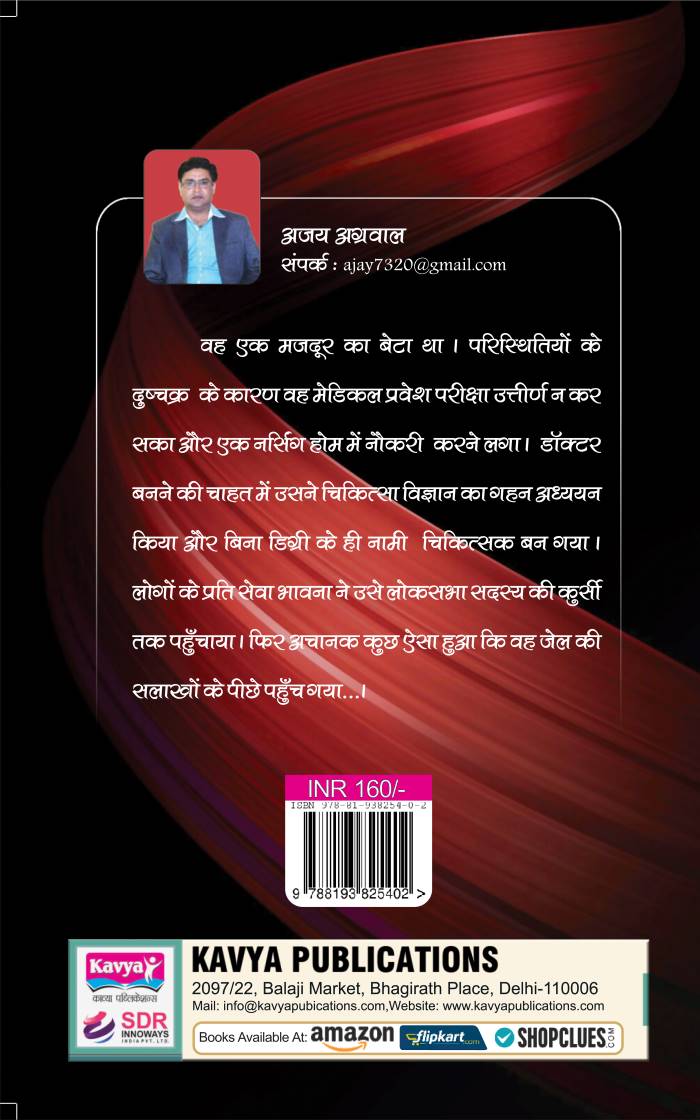
धुन्ध में दबंगई को लेकर प्रहार है. दबंगई धुन्ध का वह बीभत्स रूप है जिसके चलते सज्जनता , ईमानदारी, अर्पण समर्पण, सदाशयता सबछूमंतर की दयनीय स्थिति में रहते हैं. उपन्यास में पत्रकारों की निष्ठा पे भी सवाल उठे हैं. वे सच्चाई नहीं छाप रहे इसलिए क्योंकि वे बिकाउ हैं. जो ऊपर से निर्देश हैं उन्हें उसी के अनुरूप उन्हें कार्य करना है, उन्हें तो वही छापना है , वही छापा जाना तय है. नरसिंह , गजराज , कुलदीप जैसे चरित्रों के लिए जेल की चौखट से अंदर बाहर आना एक आम बात है. समाज में विकृतियों के स्वर इन्हीं या इन जैसे लोगों की वज़ह से हैं. इन्हीं लोगों की वज़ह से ज्योति क्लीनिक जिसने भले ही ज्योति अस्पताल की शक्ल ले ली है अधर की स्थिति में रहने के लिए बाध्य है. भले ही कालांतर इसके साथ सुन्दरी या भगवंता जैसे चारित्रिक नाम जुड़ जाएं जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के जीवंत प्रतीक हैं , जिन्होंने अपने जीवन की उष्मा को अपने बच्चे के लिए न्यौच्छावर इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बच्चा मानवता के लिए हित के लिए कुछ करना चाहता है. बच्चे ने भी तो अपने कर्तव्य की पूर्ति की ओर कदम बढ़ाया , उनकी नाम की सार्थकता को अपने मिशन के साथ जोड़कर ! लेकिन ऐसा समझने के लिए भी तो देखने वाली आंखें चाहिए.
सवाल हैं ,पर प्रखर रूप से खुलकर सामने नहीं आ पाते क्योंकि अक्सर विवशताओं से घिरे रहते हैं , ऐसे चरित्रों से घिरे रहते हैं जो समाज का अभ्युदय होते देखना नहीं चाहते. एक जमात ऐसे चुनिंदा लोगों की है जो सामाजिक समूहों को समन्याय मिलते देखना नहीं चाहती. एक भीड़ भले ही मौजूद है जिसमें बीच-बीच में जोश उमड़ता घुमड़ता भी है लेकिन ठंडा पड़ता जाता है. मुस्कान है लेकिन थकी हुई सी, परास्त हुई सी हास्य है लेकिन व्यंग्य लिए हुए. जिजीविषा है लेकिन उसके चारों ओर सत्ता के गिद्ध अपना डेरा डाले हुए हैं. प्रशासन और कानून भी तो अंततोगत्वा इन्हीं के इशारों से संचालित हैं. लेखक अपनी शिक्षकीय चेतना और दृष्टि से ये सारी परिस्थिति देख रहा है .
पहले पन्ने से आखिरी पंक्ति तक नैरंतर्य उपन्यास की रोचकता को बढ़़ाए रखता है. न इसकी गति मंद पड़ती है और न ही जिज्ञासा का स्वर ही. एक उत्सुकता निरंतर बनी रहती है. आगे क्या ? कौन परास्त होगा ? कौन विजयी होगा ? सीधी-साधी भाषा में उकेरी गई यह कृति नईहिंदी की आवश्कताओं को रेखांकित करने में पूर्णतया सफल रहीं है और यही इसकी विशेषता है. निष्कर्ष: धुन्ध से मुक्त हुए बिना स्वतंत्रता की परिकल्पना निर्मूल है. कथा ठिठकी है क़ानूनी मुद्दों की पड़ताल में फिर आगे बढ़ती है , भारतीय मंझोले कस्बाई मानसिकता के शहरों के बिम्बों को सामने रखती है. जो कम से कम हमारे हिन्दीभाषी क्षेत्रों का तकलीफदायक सच बन चुका है.
आभास